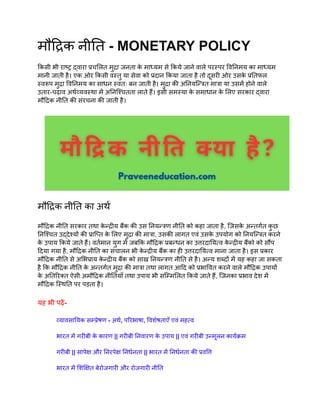
मौद्रिक नीति - MONETARY POLICY.pdf
- 1. मौद्रिक नीति - MONETARY POLICY किसी भी राष्ट्र द्वारा प्रचलित मुद्रा जनता क े माध्यम से किये जाने वाले परस्पर विनिमय का माध्यम मानी जाती है। एक ओर किसी वस्तु या सेवा को प्रदान किया जाता है तो दूसरी ओर उसक े प्रतिफल स्वरूप मुद्रा विनिमय का साधन स्वतः बन जाती है। मुद्रा की अनियन्त्रित मात्रा या उसमें होने वाले उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता लाते हैं। इसी समस्या क े समाधान क े लिए सरकार द्वारा मौद्रिक नीति की संरचना की जाती है। मौद्रिक नीति का अर्थ मौद्रिक नीति सरकार तथा क े न्द्रीय बैंक की उस नियन्त्रण नीति को कहा जाता है, जिसक े अन्तर्गत क ु छ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति क े लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत एवं उसक े उपयोग को नियन्त्रित करने क े उपाय किये जाते हैं। वर्तमान युग में जबकि मौद्रिक प्रबन्धन का उत्तरदायित्व क े न्द्रीय बैंको को सौंप दिया गया है, मौद्रिक नीति का संचालन भी क े न्द्रीय बैंक का ही उत्तरदायित्व माना जाता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति से अभिप्राय क े न्द्रीय बैंक को साख नियन्त्रण नीति से है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति क े अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत आदि को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों क े अतिरिक्त ऐसी अमौद्रिक नीतियाँ तथा उपाय भी सम्मिलित किये जाते हैं, जिनका प्रभाव देश में मौद्रिक स्थिति पर पड़ता है। यह भी पढ़ें- व्यावसायिक सम्प्रेषण - अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व भारत में गरीबी क े कारण || गरीबी निवारण क े उपाय || एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी || सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता || भारत में निर्धनता की प्रवत्ति भारत में शिक्षित बेरोजगारी और रोजगारी नीति
- 2. बेरोजगारी क े दुष्परिणाम एवं बेरोजगारी को नियंत्रित करने क े सुझाव भारत में बेरोजगारी क े कारण और बेरोजगारी कम करने क े उपाय बेरोजगारी का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, एवं भारत में बेरोजगारी की विशेषताएं मौद्रिक नीति की परिभाषाएँ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक नीति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है- पॉल एजिंग क े अनुसार- "वे सब मौद्रिक निर्णय एवं उपाय जिनक े उद्देश्य मौद्रिक हों या अमौद्रिक तथा वे सब मौद्रिक निर्णय तथा उपाय जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली पर पड़ता है, सम्मिलित होते हैं। " रेडक्लिफ समिति क े अनुसार- "मौद्रिक उपाय किसी अलग नीति का निर्णय करने की जगह एक सामान्य आर्थिक नीति, जिसक े यन्त्रों में राजकोषीय एवं मौद्रिक उपाय तथा प्रत्यक्ष नियन्त्रण सम्मिलित होते हैं, का ही एक अंग होते हैं। " प्रो. हैनरी जॉनसन क े शब्दों में- "मौद्रिक नीति, एक ऐसी नीति है, जिसक े द्वारा क े न्द्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति की प्राप्ति क े लिए मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रण में रखता है।" उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था क े विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। तथा स्वयं उनक े द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए मौद्रिक अर्थशास्त्र का अध्ययन क े वल मुद्रा क े अध्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि कीमत एवं मजदूरी नियन्त्रण, व्यापार एवं विनियोग नियन्त्रण एवं बेरोजगारी को समाप्त करने, बजट नीति, आय नीति सम्बन्धी वे अमौद्रिक उपाय भी मौद्रिक नीति में सम्मिलित किये जाते हैं। मौद्रिक नीति क े उद्देश्य एवं महत्व किसी भी राष्ट्र की मौद्रिक नीति का उद्देश्य, देश की स्थिरता को बनाये रखते हुए आर्थिक विकास करना होता है। अतः मौद्रिक नीति क े उद्देश्य या महत्व को अग्र प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है- पूर्ण रोजगार की व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार तथा आय में उच्च स्तर प्राप्त करने क े लिए मौद्रिक नीति क े द्वारा उत्पादन क े साधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त किया जाता है।
- 3. बचतों में वृद्धि होना जब मौद्रिक नीति की सफलता राष्ट्र क े प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की स्थिति में ला देती है तो स्वाभाविक है कि निवेशों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश को आर्थिक विकास क े लिए एक बड़ी राशि प्राप्त होती है। आय में स्थिरता लाना देश की वणिक व्यवस्था क े अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले व्यापार चक्रों तथा तेजी-मन्दी क े समय मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यक्तियों की आय में स्थिरता बनाये रखना होता है। विनिमय दरों में स्थिरता लाना विश्व की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा घोषित मौद्रिक नीति का मूल उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व रखना होता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी स्थिरता आती है। तीव्र आर्थिक विकास मौद्रिक नीति देश क े विकास क े लिए वित्तीय साधनों में वृद्धि करक े एवं उनकी लागतों को हटाकर उद्योग को नियन्त्रित करती है, जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यही विकास प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करता है तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था क े विकास को बढ़ावा देता है। मुदा को तटस्थ बनाना मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था क े अन्तर्गत होने वाले असन्तुलनों तथा उतार-चढ़ाव से उत्पन्न स्थिति से निबटने क े लिए मुद्रा की मात्रा को इस प्रकार नियन्त्रित करना होता है कि मुद्रा की पूर्ति भी सही बनी रहे और अर्थव्यवस्था में सन्तुलन एवं स्थिरता बनी रहे। साख-सुविधाओं का विस्तार विकासशील राष्ट्र कृ षि पर अधिक निर्भर होते हैं और गरीबी भी उनमें अधिक पायी जाती है। अतः उनक े जीवन स्तर को सुधारने तथा कृ षि क्षेत्र को बढ़ावा देने क े दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति क े माध्यम से उन्हें साख-सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। विविध उद्देश्य
- 4. एक अच्छी तथा सफल मौद्रिक नीति क े माध्यम से उपर्युक्त उद्देश्यों क े अलावा और भी निम्नांकित उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं- (1) क ु शल भुगतान यन्त्र की व्यवस्था में आसानी रहती है। (2) विदेशी विनिमय कोषों में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। (3) प्राथमिक एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएँ मिलती हैं। (4) विदेशी विनिमय की दरों में स्थायित्व स्थापित होता है। (5) आर्थिक विकास क े लिए वित्तीय साधनों की पूर्ति सम्भव होती है। (6) पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है, जिससे देश को एक सुदृढ़ बैंकिं ग आधार प्राप्त होता है। भारतीय मौद्रिक नीति क े उपकरण भारतीय क े न्द्रीय बैंक अर्थात्रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सन्1952 में नियन्त्रित साख विस्तार की नीति अपनायी थी, जिसक े प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित थे - (1) मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करना। (2) राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति जीवन स्तर में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। (3) विकास कार्यों क े लिए साख का विस्तार करते हुए योजनाओं की प्राथमिकता क े अनुरूप, साख की दिशा को निर्धारित करना था। उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ति निमित्त, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों क े साथ सहयोग लेते हुए निम्न कदम उठाये हैं- साख पर नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक ने साख नियन्त्रण की नीति क े अन्तर्गत गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों क े माध्यम से मुद्रा की माँग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न निरन्तर किया है। बैंक ने इसक े निम्न उपकरणों या उपायों को प्रयोग में लिया है
- 5. (i) नकद कोषानुपात में परिवर्तन इसक े अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने साख नियन्त्रण करने क े लिए यह नियम प्रतिपादित कर रखा है कि देश क े प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक को निक्षेप करना होता है जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है। तो रिजर्व बैंक, बैंकों की दर में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता स्वतः ही कम हो जाती है। जब यह क्षमता बढ़ानी होती है तो नकद कोष में जमा किये जाने वाले धन की दर को घटा दिया जाता है तो उतनी राशि, बैंकों क े पास साख निर्माण क े लिए बढ़ जाती है। वर्तमान में नकद कोषानुपात 4% की दर पर है। (ii) सम्पूर्णतया फ ै लाव की प्रवृत्ति मौसम एवं मुद्रा की बढ़ती हुई लागत क े अनुरूप मुद्रा की आपूर्ति में घट-बढ़ क े बावजूद क ु ल मिलाकर मुद्रा पूर्ति की प्रवृत्ति फ ै लाव की ओर रही है। इसक े साथ ही सामान्य मूल्य स्तर में भी लगभग निरन्तर वृद्धि होती रही है। जब राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की पूर्ति अधिक तेजी से बढ़ती है तथा सामान्य मूल्य स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यह स्फीति का संक े तक है और माप भी है। मुद्रा पूर्ति में यह वृद्धि मुख्यतः शासन द्वारा भारी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेने का परिणाम है। मुदा फ ै लाव को सम्भव बनाने क े लिए रिजर्व बैंक की रिजर्व प्रणाली में परिवर्तन किया गया। प्रणाली की सख्ती को दूर करक े इसे लचीला बनाया गया। इस ध्येय से आनुपातिक रिजर्व प्रणाली हटा दी गयी। अब रिजर्व बैंक अपने पास रखे रिजर्व की निम्नतम मात्रा में वृद्धि बिना वांछित परिणाम में रुपये निर्गमित कर सकता है। (iii) महँगी मुद्रा मुद्रा पूर्ति की विस्तार प्रवृत्तियों पर रिजर्व बैंक ने सख्त दृष्टि रखी। जहाँ बढ़ती हुई आवश्यकताओं क े अनुरूप मुद्रा पूर्ति क े फ ै लाव क े लिए प्रणाली में लचीलेपन की आवश्यकता थी। वहाँ रिजर्व बैंक इस पर रोक लगाने क े लिए प्रयास करती रही। हालांकि रिजर्व बैंक सदैव इस कार्य में सफल नहीं रहा। यह स्थिति इस कारण पैदा हुई है कि जहाँ एक ओर उन क्षेत्र क े लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी थी जिनकी संवृद्धि राष्ट्र क े आर्थिक विकास क े लिए जरूरी थी, वहीं दूसरी ओर मुद्रा प्रसार को रोकना जरूरी था, ताकि स्फीतिकारी शक्तियाँ अधिक प्रबल न होने पाएँ। इस विरोध को दूर करने क े लिए रिजर्व बैंक ने सामान्य और याचनात्मक नियन्त्रण तकनीक का विकास किया। उधार पात्रता और उधार नियन्त्रण स्कीमों क े द्वारा बन्धन लगाने क े साथ-साथ ब्याज की दर में वृद्धि की गयी। मुद्रा नीति क े इन दोनों पहलुओं क े फलस्वरूप और अभी हाल तक यह नीति बनी रही, मुद्रा नीति स्फीति विरोधी थी और इसे कठोर एवं महँगी मुद्रा नीति की संज्ञा दी गयी। (iv) निवेश और बचत उन्मुखता विगत क ु छ वर्षों से मुद्रा नीति को निवेश और बचत को बढ़ावा देने क े उद्देश्य की ओर उन्मुख कर दिया गया है। क ु छ वर्ष पहले तक नीति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की लागत संरचना को नीचे की ओर झुकाना था। उधार नियन्त्रण क े उपायों को अपनाते हुए, इस उद्देश्य क े पालन में निवेश की लागत कम करने क े
- 6. लिए उधार दर घटा दी गयी। इस प्रकार मुद्रा नीति मुद्रा की पूर्ति और उपलब्धता को नियन्त्रित करने वाली बनी रही, लेकिन मुद्रा उपलब्ध कराने की शर्तों को थोड़ा आसान कर दिया गया। नवीनतम और वर्तमान चरण में बचतों को पूँजी बाजार में स्थानान्तरित करने क े लिए बैंक ब्याज दर घटायी जा रही है। मौद्रिक नीति की विषय-सामग्री रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य राष्ट्र की मौद्रिक एवं साख संरचना को नियन्त्रित करना होता है। रिजर्व बैंक आरम्भ से ही नियन्त्रित मौद्रिक विस्तार की नीति अपनाता रहा है, जिसक े अन्तर्गत विकासार्थ वित्त व्यवस्था करना तथा अन्य राष्ट्रों क े मूल्यों का अध्ययन कर स्वयं की मूल्य स्थिरता पर ध्यान क े न्द्रित करना है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की विषय-सामग्री में निम्नलिखित चार मुख्य विषय शामिल हैं- समुचित व्याज दर नीति रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति में महँगी मुद्रा नीति अपनायी। इस दृष्टि से 1930-40 क े दशक में 3 प्रतिशत की बैंक दर अपनायी गयी जो 1953 तक यही रही, फिर इसे बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत जुलाई 1981 तक इसे 10 प्रतिशत, जुलाई 1999 तक 11 प्रतिशत, अक्टूबर 1991 तक बढ़कर 12 प्रतिशत कर दिया गया जिसे कि महँगी मुद्रा माना जाता है किन्तु पुनः इसे 2000 से घटाना आरम्भ कर 2002 में 6 प्रतिशत तक लाया गया, जिसे सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। फरवरी 2015 को बैंक दर 8.75% थी। बैंक दर या रिजर्व बैंक की पुनः बट्टा दर तथा बैंकों की जमा दरें आधुनिक अर्थव्यवस्था क े महत्वपूर्ण मौद्रिक उपाय हैं। यदि मौद्रिक नीति प्रभावी एवं विश्वसनीय है तो बैंक दर में परिवर्तन क े फलस्वरूप बैंकों की प्राथमिक उधार दर में परिवर्तन होगा। इस प्रकार यह एक स्वतन्त्र मौद्रिक नियन्त्रण क े उपाय क े रूप में कार्य करेगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। भारत में बैंक दरों क े लिए गति निर्धारक का कार्य नहीं करती। मौद्रिक बाजार दरें स्वतः बैंक दर में परिवर्तन क े साथ परिवर्तित नहीं होती। उधार दरें भी बैंक दर से नहीं जुड़ी हैं। शासन एवं आर. बी. आई. दोनों प्रयासरत हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की भाँति बैंक दर को मौद्रिक नीति का सक्रिय उपकरण बनाया जा सक े । वित्तीय संस्थाओं का विस्तार रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं क े विस्तार में महती भूमिका का निर्वहन किया है। उसने कृ षि तथा औद्योगिक विकास बैंक आफ इण्डिया, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय कृ षि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं निर्यात बैंक की स्थापना उस दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण बैंकिं ग सुविधाओं की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जाल भी बिछाया है। साख सुविधाओं का विस्तार
- 7. इस दृष्टि से रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय अपनाये- (i) निर्यात विनिमय प्रपत्र साख योजना का आरम्भ (1963), (ii) खुले बाजार की क्रियाओं में संशोधन एवं बिल बाजार को उदार बनाना (1957), (iii) विभेदक व्याज पर योजना का लागू करना (1972), (iv) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। मुद्रा की माँग एवं पूर्ति में सन्तुलन आर्थिक विकास कार्यक्रम क े समुचित संचालन हेतु रिजर्व बैंक हमेशा मुद्रा की माँग एवं आपूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने का कार्य करता है। यदि मुद्रा की अधिकता होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार क े दोष उत्पन्न होते हैं। वास्तव में प्रथम योजना को छोड़कर अभी तक रिजर्व बैंक अपने इस कार्य में सफल नहीं रहा। बैंकिं ग नीति और प्रवृत्तियाँ चालू वित्तीय वर्ष क े दौरान बैंकिं ग क्षेत्रक में चालू सुधारों का ध्यान क े न्द्रण उदार शर्तों पर ब्याज दर प्रणाली, बैंकों की प्रचलनात्मक क्षमता बढ़ाने, विनियामक तन्त्र सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर था। अधिक उदार शर्तों पर ब्याज दर प्रणाली की ओर अग्रसर होने क े रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक नीति विवरण में बैंकों से नई जमाराशियों क े लिए लचीली व्याज दर प्रणाली लागू करने, उपभोक्ता ऋण को छोड़कर सभी अग्रिमों क े लिए पीएलआर पर अधिकतम ऋण को छोड़कर सभी अग्रिमों क े लिए पीएलआर पर अधिकतम विस्तार घोषित करने और पीएलआर पर वर्तमान अधिकतम विस्तार की समीक्षा करने तथा जहाँ भी वे अनुचित रूप से अधिक हैं, उन्हें कम करने का सुझाव दिया था। बैंक दर में परिवर्तन बैंक दर से आशय, उस दर से है जिस पर रिजर्व बैंक, बैंकों को ऋण प्रदान करता है या उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती करता है। इस दर क े बढ़ने पर बैंक ऋणों की लागत बढ़ने से, बैंक उधार कम देने की स्थिति में आ जाता है और साख की मात्रा घट जाती है। ऊ ँ ची बैंक दर को महँगी साख नीति तथा निम्न दर को सस्ती साख नीति कहा जाता है। फरवरी, 2015 को बैंक दर 8.7 प्रतिशत थी। वैधानिक तरल कोषानुपात परिवर्तन
- 8. इस विधि में, बैंकिं ग कम्पनीज एक्ट, 1949 क े अनुरूप यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक बैंक अपनी क ु ल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने ही पास तरल कोषों क े रूप में रखेगा, जिससे कि यथास्थिति साख पर नियन्त्रण रखा जा सक े । SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जो 25 से 40% क े बीच होता है। परन्तु वर्ष 2007 से इसकी न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। SLR का मुख्य उद्देश्य बाजार में मुद्रा क े प्रसार को नियन्त्रित करना होता है। इसक े अधिक होने से बाजार में मुद्रा का प्रसार कम होता है तथा कम होने से मुद्रा का प्रसार अधिक होता है। फरवरी, 2015 को SLR 21.50% थी। उपभोक्ता साख नियन्त्रण इस उपकरण क े द्वारा रिजर्व बैंक जब यह देखता है कि मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं की माँग घट रही है तो वह अग्रिमों को घटाता है, जबकि माँग में कमी होते ही उस माँग को बढ़ाने क े लिए उपभोक्ताओं को कम दर पर ऋण सुविधा देना प्रारम्भ कर देता है। चयनित साख नियन्त्रण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस उपकरण क े माध्यम से निम्नलिखित चयनित साख नियन्त्रण करता है- (i) कम्पनियों की ऋण नीति को निर्धारित कर सकता है। (ii) ऋणों क े उद्देश्य तथा अधिकतम ऋण एवं गारण्टी की राशि को निश्चित कर सकता है। (iii) ऋणों की ब्याज दर, कटौती की दर, मूल्यान्तर निर्धारण एवं ऋणों पर प्रतिबन्धादि की कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान में दी गयी व्यवस्था क े अनुसार रिजर्व बैंक ने समस्त व्यापारिक बैंकों को यह आदेश प्रसारित किया हुआ है कि वे अपने क ु ल ऋण एवं अग्रिमों का कम से कम 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ही देंगे। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन देश में सुदृढ़ बैंकिं ग व्यवस्था होने पर ही मौद्रिक नीति की सफलता निर्भर करती है और इसलिए, इस सन्दर्भ में भारत में, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त एवं निवेश निगम, राज्य वित्त निगम तथा भारतीय इकाई प्रन्यास जैसे दीर्घकालीन निगमों एवं वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी है। विकासशील राष्ट्रों में मौद्रिक नीति की सीमाएँ
- 9. विकासशील राष्ट्रों क े आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु विकासशील राष्ट्रों की संरचनात्मक विशेषताओं क े कारण वहाँ मौद्रिक नीति क े सफल प्रयोग का क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहता है। विकासशील राष्ट्रों में मौद्रिक नीति क े पूर्ण रूप से प्रभावशील न होने क े कारण निम्नलिखित हैं- मौद्रिक नीति का सीमित क्षेत्र (i) विशाल अमौदिक क्षेत्र विकासशील राष्ट्रों में एक विशाल अमौदिक क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ मुद्रा का चलन नहीं होता बल्कि विनिमय की अदला-बदली पद्धति ही प्रचलित है, फलत: इन क्षेत्रों में मुद्रा की मात्रा या ब्याज की दर सम्बन्धी परिवर्तन आर्थिक क्रियाओं क े परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इस प्रकार मौद्रिक नीति का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। (ii) साख मुद्रा का कम महत्व विकासशील राष्ट्रों में साख मुद्रा क े स्थान पर चलन मुद्रा अधिक महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए रिजर्व बैंकों की साख पर नियन्त्रण लगाने पर भी मुद्रा की पूर्ति पर नियन्त्रण नहीं हो पाता। मौद्रिक नियन्त्रण का सीमित प्रभाव (i) संगठित मुद्रा बाजार का अभाव विकासशील राष्ट्रों में असंगठित मुद्रा बाजार का अभाव रहता है, अतः बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं एवं बैंक कोष में परिवर्तन का राष्ट्र की साख व्यवस्था पर प्रभावशाली महत्व नहीं रहता। उदाहरणार्थ, बैंक दर बढ़ाने से भी उन राष्ट्रों में साख का संक ु चन नहीं हो पाता क्योंकि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक क े ऊपर आश्रित नहीं होते। व्याज दर बढ़ने से इन बैंकों पास जमा राशि बढ़ जाती है, इस कारण वे अपने साख निर्माण का कार्य पूर्ववत्करते रहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएँ भी अधिक सफल नहीं होतों क्योंकि इन राष्ट्रों में राज्य की प्रतिभूतियों का बाजार अविकसित होता है। इसी तरह, रिजर्व बैंक क े द्वारा न्यूनतम कोष सीमा बढ़ाने से भी इन राष्ट्रों में साख का संक ु चन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बैंकिं ग क े बहुत से सौदे नकद में हो होते हैं और इस कारण बैंक सामान्यतः इस न्यूनतम सीमा से कहीं अधिक नकद कोष रखते हैं, फलतः यदि रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष की सीमा बढ़ाते भी हैं तो उसक े लिए साख का संक ु चन नहीं करना पड़ता। (ii) बिल बाजार का अभाव विकासशील राष्ट्रों में प्रायः विकसित एवं सामान्य कटौती बाजार का अभाव होता है, जिसक े कारण साख प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पाती।
- 10. (iii) अन्य कारण विकासशील राष्ट्रों में मौद्रिक नियन्त्रण क े सीमित प्रभाव क े अन्य कारण हैं- (अ) निजी बैंकिं ग प्रणाली का क े न्द्रीय बैंकिं ग क े नियन्त्रण क े क्षेत्र से बाहर होना। (ब) सदस्य बैंक और रिजर्व बैंक क े मध्य प्रभावपूर्ण सहयोग का होना। उपर्युक्त कारणों से ही यह कहा जाता है कि विकासशील राष्ट्र में आर्थिक विकास को द्रुत करने क े लिए अपनायी गयी मुद्रा नीति निश्चित रूप से निष्फल होती है। यद्यपि एक विकासशील राष्ट्र क े विकास में मौद्रिक नीति का क्षेत्र उक्त कारणों से अत्यन्त सीमित होता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विकासशील राष्ट्रों में इसकी कोई भूमिका नहीं है। यह सत्य है कि आर्थिक विकास की भारी समस्या क े वल मौद्रिक तोड़-फोड़ से ही सुलझायी नहीं जा सकता क्योंकि आर्थिक विकास मौद्रिक घटकों घर ही नहीं वरन्वास्तविक घटकों, यथा- श्रम, पूँजी, भूमि, संगठन व साहस क े रूप में उपलब्ध होने वाले प्रसाधनों पर निर्भर होता है। मौद्रिक नीति, साख की पूर्ति और उसक े प्रयोग को प्रभावित करक े , मुदा प्रसार का सामना करक े व भुगतान सन्तुलन में साम्यता बनाये रखकर आर्थिक विकास में बड़ी सहायता कर सकती है। यहीं कारण है कि मौद्रिक नीति नियोजित आर्थिक विकास का आधारभूत यन्त्र मानी जाती है। मौद्रिक नीति की असफलताओं क े कारण रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण में निम्नलिखित कारणों से असफल प्रतीत होता है- मौद्रिक लक्ष्यों का निर्धारण न होना मुद्रा आपूर्ति, उत्पादन एवं मूल्यों में परस्पर सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों क े आधार पर ही मौद्रिक नीति सफल होती है। विगत दो दशकों में मौदिक आपूर्ति उत्पादन वृद्धि पर आश्रित न होकर सरकारी उधार की माँग पर आश्रित है, अतः मौद्रिक नीति असफल रही है। काले धन का प्रवाह एक अनुमान क े अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी. एन. पी. क े 30 से 40 प्रतिशत क े बराबर काला धन अर्थव्यवस्था में प्रवाहित है। इससे मौद्रिक नीति का परिपूर्ण पालन असफल हो रहा है। वित्तीय अनुशासन का अभाव
- 11. व्यापारिक बैंकों द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाये जाने से साख विस्तार क े फलस्वरूप जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। पूँजी बाजार की भूमिका पूँजी बाजार में कई सौदे मूल्य स्तर पर दबाव डालते हैं; यथा- राष्ट्रीय बचत पत्र पर ऋण, बीमा पॉलिसी पर ऋण आदि । मुद्रा बाजार का धीमा विकास भारत का मुद्रा बाजार अभी भी पूर्णतया विकसित नहीं है, अतः मौद्रिक नीति अप्रभावी रह जाती है। रिजर्व बैंक का सम्मिलित कार्य क्षेत्र आर. बी. आई. का कार्यक्षेत्र क े वल बैंकों तक है, अतः आर. बी. आई. की हीनता प्रबन्धन आदि पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का उपयोग इससे स्थिति विवरण का आकार सिक ु ड़ रहा है, जिससे मौद्रिक नीति एक चुनौती बन जायेगी। गैर-बैंकिं ग संस्थाओं पर अनियन्त्रण आर. बी. आई. का गैर-बैंकिं ग संस्थाओं पर नियन्त्रण न होने से मौद्रिक नीति क े संचालन में असुविधा होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मौदिक संकट अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट क े कारण भी आर. बी. आई. को क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बैंकों क े पास नकद कोषों की अधिकता बैंकों में जमा वृद्धि से शुद्ध तरलता अनुपात बैंकों की साख की फ ै लाव क्षमता को प्रभावित नहीं करते।